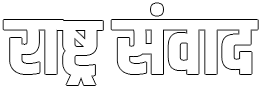क्या धर्मनिरपेक्षता से इस्लामिक राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहा बांग्लादेश ?
देवानंद सिंह
बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास और विकास की यात्रा पर नज़र डालें तो यह कई परतों से सजी हुई है। पाकिस्तान के गठन के समय से लेकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम और फिर उसके बाद के घटनाक्रमों ने यह साबित किया है कि राष्ट्रवाद एक गतिशील और बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसे समझने के लिए हमें इतिहास, धर्म, संस्कृति और राजनीति की जटिलता को ध्यान में रखना होगा। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की बुनियाद बांग्ला राष्ट्रवाद थी, लेकिन क्या इस राष्ट्रवाद में धर्मनिरपेक्षता की जगह अब इस्लामिक राष्ट्रवाद ने ले ली है? यह सवाल आज भी प्रासंगिक है और समय के साथ इसकी महत्ता बढ़ी है।
बांग्लादेश की उत्पत्ति 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर हुई थी, जब बांग्लादेशियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के लिए संघर्ष किया। बांग्ला राष्ट्रवाद का आधार मुख्य रूप से भाषा और संस्कृति पर आधारित था। पाकिस्तान में उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के बाद, बांग्लादेश में भाषायी पहचान के लिए संघर्ष ने बांग्ला राष्ट्रवाद को जन्म दिया। मार्च 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा घोषित किए जाने के बाद, बांग्लादेश में भाषायी आंदोलन ने जोर पकड़ा था। 1952 में पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषा के अधिकार के लिए हुआ संघर्ष, जो अब ‘भाषा आंदोलन’ के नाम से जाना जाता है, बांग्ला राष्ट्रवाद के सिद्धांत को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम था। यह आंदोलन एक तरह से बांग्लादेश की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया और बांग्ला संस्कृति की महत्ता को रेखांकित किया। 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में इसी पहचान की अहम भूमिका थी। शेख़ मुजीब-उर रहमान ने बांग्लादेश के निर्माण की बुनियाद इस विश्वास पर रखी कि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिलेंगे।
बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता के बाद धर्मनिरपेक्षता को अपनाया था, लेकिन 1975 में शेख़ मुजीब-उर रहमान की हत्या और सैन्य तख़्तापलट ने स्थिति को पूरी तरह बदल दिया। सैन्य शासन के दौरान, ज़िआ-उर रहमान ने 1977 में संविधान से धर्मनिरपेक्षता की धारा हटा दी और इस्लामिक पार्टियों पर लगी पाबंदी को भी हटा लिया। 1988 में जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने इस्लाम को बांग्लादेश का राजकीय धर्म घोषित कर दिया। हालांकि, 2009 में शेख़ हसीना के नेतृत्व में अवामी लीग की सरकार ने संविधान में फिर से धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने का वादा किया और 2011 में इसे पुनः लागू किया। फिर भी, बांग्लादेश में इस्लाम के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। बांग्लादेश का संविधान इस्लाम को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता देता है, लेकिन साथ ही यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का भी दावा करता है। बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 12 में यह स्पष्ट किया गया है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को बनाए रखा जाएगा और सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए जाएंगे।
हाल ही में बांग्लादेश में इस्लामिक ताकतों के उभार ने बांग्ला राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को चुनौती दी है। बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक पार्टियां, जैसे जमात-ए-इस्लामी, जो पाकिस्तान के पक्ष में रही हैं, अब बांग्लादेश की राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। इस्लामिक ताकतों के बीच यह प्रयास है कि बांग्लादेश को इस्लामी राज्य के रूप में रूपांतरित किया जाए।
विशेष रूप से 1980 के दशक में खाड़ी देशों में काम करने गए बांग्लादेशी श्रमिकों ने एक अलग प्रकार का इस्लाम देखा। सऊदी अरब जैसे देशों से आई मदरसों और इस्लामी शिक्षा ने बांग्लादेश की राजनीति में भी बदलाव लाया। इस इस्लाम का प्रभाव बांग्लादेश के समाज में गहरे तौर पर पैठ गया और बांग्ला राष्ट्रवाद का इस्लाम से टकराव शुरू हो गया। शेख़ हसीना के जाने के बाद, बांग्लादेश में इस्लामी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला और कई धार्मिक मुद्दों पर विवाद उठने लगे।
बांग्लादेश में आज भी इस बात पर बहस जारी है कि क्या बांग्ला राष्ट्रवाद अब इस्लामिक राष्ट्रवाद से परे हो गया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेशी समाज अब भी अपने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है। बांग्लादेशी समाज ने पाकिस्तान से अलग होने के बाद अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष में धर्मनिरपेक्षता की अहमियत को समझा था और आज भी बांग्लादेश के लोग अपने अतीत को नहीं भूल सकते, खासकर उस दौर को जब धर्म के नाम पर अत्याचार हुए थे। हालांकि, बांग्लादेश में आज भी इस्लाम के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ावा देने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन बांग्लादेशी समाज की संरचना और संस्कृति इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश की महिलाएं, जो पाकिस्तान की महिलाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा आधुनिक और स्वतंत्र हैं, इसका प्रमाण हैं। बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच सहयोग और समन्वय भी पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है।
कुल मिलाकर, बांग्लादेश का राजनीतिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अब भी गतिशील है और भविष्य में यह कई मोड़ ले सकता है। बांग्ला राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता की नींव पर खड़ा बांग्लादेश आज इस्लामिक राष्ट्रवाद की चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश के जो लोग पाकिस्तान के साथ अपने अनुभवों से गुजरे हैं, शायद अपने देश की भविष्यवाणी करने में जल्दबाजी न करें। बांग्लादेश का लोकतंत्र और समाज की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि यह बदलावों के बावजूद अपनी अस्मिता और पहचान को बनाए रखने में सक्षम रहेगा। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि बांग्लादेश के लोग अपने इतिहास से शिक्षा लेकर ही आगे बढ़ेंगे और जो गलतियां पाकिस्तान ने धार्मिक राष्ट्रवाद के नाम पर की थीं, उनसे बचने का प्रयास करेंगे। बांग्लादेश का भविष्य एक ऐसे राष्ट्र के रूप में है, जो अपनी बांग्ला पहचान को महत्व देता है और जहां धर्मनिरपेक्षता और धार्मिकता के बीच एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।