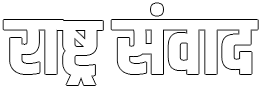बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के मायने
देवानंद सिंह
बिहार में इस वर्ष के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक जटिल विवाद का रूप ले चुका है। लोकतंत्र का यह मूलभूत उपकरण, जो नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, अब एक गहन प्रशासनिक एवं नीतिगत उलझन में उलझा हुआ प्रतीत होता है। इस संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप न केवल समयोचित बल्कि लोकतांत्रिक सरोकारों से प्रेरित एक संवेदनशील पहल के रूप में देखा जाना चाहिए।

चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत वोटर लिस्ट से फर्जी नाम हटाने और नए नाम जोड़ने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक गूढ़ विवाद तब पैदा हुआ, जब आयोग ने केवल निवास प्रमाण पत्र को ही वैध दस्तावेज़ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया, इससे यह आशंका उत्पन्न हुई कि जिन नागरिकों के पास यह विशेष दस्तावेज़ नहीं है, उन्हें या तो सूची से बाहर कर दिया जाएगा, या उन्हें नाम जोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस एक निर्णय ने पूरे राज्य में दस्तावेज़ीय असमानता और प्रशासनिक भ्रम की एक सुनामी ला दी।

किशनगंज जिले की बात करें तो एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, मात्र एक सप्ताह में दो लाख से अधिक निवास प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन दायर किए गए हैं। यह संख्या यह दर्शाती है कि या तो नागरिकों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं थी, या फिर अपेक्षित दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता एक सामान्य चुनौती है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या लोकतंत्र में भागीदारी की शर्त केवल कागज़ी सबूतों तक सीमित हो सकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे का स्वत: संज्ञान नहीं लिया, बल्कि यह मामला तब उनके समक्ष आया, जब नागरिकों और सामाजिक संगठनों की ओर से चिंता प्रकट की गई कि इस विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्यायसंगतता की भारी कमी है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी को सहायक दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

यह सुझाव किसी भी प्रकार से विधिक व्यवस्था के साथ समझौता नहीं है, बल्कि यह उस वास्तविकता की स्वीकारोक्ति है, जिसमें देश की एक बड़ी आबादी अभी भी दस्तावेज़ीय असमानता और प्रशासनिक अपारदर्शिता का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नाम काटने की प्रक्रिया को इतनी सहजता से नहीं अपनाया जाना चाहिए, खासकर तब जब एक बार नाम हट जाने के बाद पुनः नाम जुड़वाना बेहद कठिन प्रक्रिया है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से ग्रस्त देश में, लोकतंत्र की आत्मा तभी जीवित रह सकती हैं, जब उसमें सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो। निर्वाचन आयोग का यह दायित्व है कि वह फर्जी नामों को हटाने के लिए कदम उठाए, परंतु उस प्रक्रिया में एक भी वास्तविक नागरिक को बाहर कर देना सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अपराध होगा।

बिहार की सामाजिक संरचना विशेष रूप से इस परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील है। यहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर, सीमावर्ती इलाकों के निवासी, जनजातीय समुदाय, मुसलमान, दलित और अशिक्षित नागरिक निवास करते हैं। उनके पास अपेक्षित दस्तावेज़ नहीं होना, इस बात का प्रमाण नहीं हो सकता कि वे बिहार के नागरिक नहीं हैं। लोकतंत्र की मूल अवधारणा कहती है कि जब तक किसी नागरिक की नागरिकता पर संदेह सिद्ध न हो, तब तक उसे उसका संवैधानिक अधिकार यानी मत देने का अधिकार नहीं छीना जा सकता।
दरअसल, समस्या सिर्फ दस्तावेज़ों की नहीं है, बल्कि नीतिगत दिशा-निर्देशों की अस्पष्टता की भी है। कई जिलों से रिपोर्ट आई है कि घर-घर सर्वेक्षण करने वाले सरकारी कर्मी स्वयं भ्रमित हैं। उन्हें यह नहीं बताया गया है कि किन दस्तावेज़ों को वैध मानना है। कुछ स्थानों पर वे केवल आधार कार्ड मांग रहे हैं, तो कुछ स्थानों पर राशन कार्ड की मांग की जा रही है। इसके अतिरिक्त, फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया में भी भारी भेदभाव और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं।

यह न केवल प्रशासनिक अराजकता को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को राजनीतिक या चुनावी दबाव में जल्दबाजी में शुरू किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात पर चिंता प्रकट की है कि क्या इस समय विशेष पर, जब चुनाव समीप हैं, इतनी व्यापक पुनरीक्षण प्रक्रिया गुणवत्ता और निष्पक्षता के साथ पूरी की जा सकेगी? भारत में दस्तावेज़ीय प्रमाणों की व्यवस्था एक विशेष प्रकार की सामाजिक-आर्थिक सुविधा का प्रतीक बन गई है। एक शहरी, शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम नागरिक के लिए आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराना अपेक्षाकृत सरल है, लेकिन वही सुविधा एक ग्रामीण, अनपढ़, प्रवासी या हाशिए पर खड़े नागरिक के लिए एक जटिल भूलभुलैया बन जाती है।

बिहार में बड़ी संख्या में नागरिकों के पास न तो डिजिटल पहचान है, न ही नियमित आधार पर अद्यतन किया गया राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र। ऐसे में, जब अचानक उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे इन दस्तावेज़ों को कुछ ही दिनों में प्रस्तुत करें, तो यह उनके लिए केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक सामाजिक संकट बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस संदर्भ में न केवल न्यायसंगत है, बल्कि वह एक संवेदनशील लोकतांत्रिक संरक्षक की भूमिका निभा रहा है। अदालत का यह सुझाव कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी को सहायक दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाए, यह एक बेहद व्यावहारिक और मानवीय समाधान है। इससे न केवल आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार होगा, बल्कि नागरिकों के मन में भी विश्वास उत्पन्न होगा कि यह प्रक्रिया किसी बहिष्करण का हथियार नहीं, बल्कि समावेश का साधन है।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भरोसा भी दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची से बिना सुने नहीं हटाया जाएगा। यह आश्वासन न केवल संवैधानिक नैतिकता के अनुकूल है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा को भी संरक्षित करता है। इस पूरी बहस का सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि लोकतंत्र की जड़ें केवल भावना में नहीं, बल्कि नीति और प्रक्रिया की स्पष्टता में भी निहित होती हैं। यदि आयोग स्पष्ट रूप से यह बता दे कि किन दस्तावेज़ों के आधार पर नाम काटे जा सकते हैं, किन दस्तावेज़ों के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं, और नागरिकों को अपनी बात रखने के लिए क्या मंच उपलब्ध हैं, तो भ्रम की स्थिति स्वतः समाप्त हो जाएगी।
इसके साथ ही, डोर-टू-डोर सर्वेक्षण के लिए नियुक्त कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उनका व्यवहार न केवल प्रशासनिक होना चाहिए, बल्कि नागरिक-सम्मान और संवेदनशीलता से भी परिपूर्ण होना चाहिए। बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव केवल एक क्षेत्रीय राजनीतिक घटना नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय राजनीति की दिशा को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि इस चुनाव में बड़ी संख्या में नागरिक मतदाता सूची से वंचित रह जाते हैं, या उन्हें मतदान से रोका जाता है, तो यह न केवल एक लोकतांत्रिक क्षति होगी, बल्कि इससे पूरे तंत्र की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लग सकता है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसी प्रक्रियाएं शुद्धिकरण का उद्देश्य लेकर शुरू होती हैं, यानी कि मतदाता सूची से फर्जी या मृत नामों को हटाना। यह उद्देश्य निश्चित रूप से उचित है, परंतु यदि इसी प्रक्रिया में असली और योग्य मतदाताओं को बाहर कर दिया जाए, तो यह लोकतंत्र का क्षरण है, शुद्धिकरण नहीं। कुल मिलाकर, भारत का लोकतंत्र आज उस मोड़ पर खड़ा है, जहां प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी नवाचार और न्यायिक विवेक, तीनों को एक संतुलित तालमेल में चलना होगा। बिहार में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण इस तालमेल की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र केवल एक संवैधानिक संरचना नहीं, बल्कि जन-समावेश की चेतना है।
आयोग को चाहिए कि वह जल्द से जल्द एक स्पष्ट, पारदर्शी और व्यावहारिक नीति घोषित करे, जिससे नागरिकों में विश्वास बहाल हो सके। सरकार को चाहिए कि वह आवश्यक दस्तावेज़ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाए, और समाज के अंतिम व्यक्ति तक यह संदेश पहुंचाएं कि वह भारतीय लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, क्योंकि अंततः, लोकतंत्र का मूल्य इस बात में नहीं कि कितने वोट डाले गए, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग बिना भय, भ्रम और बाधा के अपने अधिकार का प्रयोग कर पाए, और यही वह कसौटी है, जिस पर आज बिहार खड़ा है।