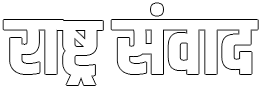ललित गर्ग
देश में आर्थिक सुस्ती एवं विकास की रफ्तार में लगातार आ रही गिरावट चिंता एवं चिन्तन का कारण है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई-सितंबर, 2019 की तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि-दर की लगातार छठी बार गिरावट होना असामान्य आर्थिक घटना है। इस तिमाही में जीडीपी दर 4.5 प्रतिशत दर्ज की गई है। गौरतलब है कि जीडीपी किसी खास अवधि के दौरान वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की कुल कीमत है। भारत में कृषि, उद्योग और सर्विसेज तीन प्रमुख घटक हैं जिनमें उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। पिछले कुछ समय से इन तीनों ही क्षेत्रों में भारी सुस्ती एवं गिरावट दिख रही है, यह सरकार की आर्थिक मोर्चे पर विफलता को दर्शाती है। महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम एवं झारखंड में होने जा रहे विधानसभाओं को देखते हुए जीडीपी का गिरना भाजपा सरकार के सेहत के लिये अच्छा नहीं है। ऐसा भी प्रतीत होता है सरकार में कोई ऐसा सक्षम एवं प्रभावी आर्थिक स्थितियों को पटरी पर लाने वाला नेतृत्व नहीं है।
अर्थव्यवस्था अजीब विरोधाभासी दौर में है जिसमें लगातार उत्पादन गतिविधियां कमजोर हो रही हैं, निवेश घट रहा है, बाजार में मांग कम हो रही है और निर्यात घाटा भी बढ़ रहा है तथा विदेशी मुद्रा डालर महंगी हो रही है मगर शेयर बाजार बढ़ रहा है और सोने की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति की दर या महंगाई में कमी को भी इन्हीं सब आधारभूत आर्थिक मानकों से बांध कर देखना होगा। इसका सीधा मतलब यह होता है कि बाजार में सक्रिय आर्थिक शक्तियां निराशा एवं हताशा की स्थिति में हैं। प्रश्न है कि यह स्थिति क्यों बन रही है? सरकारी बजट को आम लोग समझते ही नहीं कि उनके धन का कितना उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। जो समझते हैं वे सिवाय विरोध के कुछ नहीं करते।
नरेन्द्र मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पिछले दिनों जो उपाय किए हैं, उनका असर अगली तिमाही से दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा विश्वास किया जा रहा है और यह जरूरी भी है। क्योंकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 6.7 फीसदी से गिरकर सिर्फ आधा प्रतिशत रह गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का तो बुरा हाल है जिसमें बढ़ोत्तरी की जगह आधे प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई है। कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर 4.9 से गिरकर 2.1 फीसदी और सर्विसेज की दर भी 7.3 फीसदी से गिरकर 6.8 ही रह गई है। मुश्किल यह है कि आम उपभोक्ताओं ने हाथ बांध रखे हैं। लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, वे अपने रोजमर्रा के खर्च में कटौती कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक भय एवं आतंक का माहौल बना हुआ है, इससे मांग पैदा हो नहीं रही है जिसके कारण उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। कारोबारी दुविधा में हैं। कंपनियों को अपना उत्पाद कम करना पड़ रहा है। उनमें से कई अपने कर्मचारियों की छंटनी करने को मजबूर हो रही हैं। दरअसल बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा न होने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गिरावट की खबरें आने, आवास परियोजनाएं फंसने, पब्लिक सेक्टर की कई कंपनियों व बैंकों के संकट में पड़ने और कई वस्तुओं की बढ़ती महंगाई ने लोगों को आशंकाओं एवं निराशाओं से भर दिया है। वे खरीदारी और निवेश से कतरा रहे हैं।
गौरतलब है कि सरकार ने विदेशी निवेशकों से सरचार्ज हटाया और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की। ऑटो सेक्टर की बेहतरी के लिए घोषणाएं की गईं, संकटग्रस्त रीयल एस्टेट और नॉन बैंकिंग फाइनैंशल कंपनियों के लिए भी कदम उठाए गए। इन सबसे बाजार में सुधार की आशा है। संभव है, बाजार में डिमांड बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक अगले हफ्ते फिर ब्याज दरें घटाए। मगर इन सबके साथ-साथ सरकार को रोजगार बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर लोगों को बड़े पैमाने पर नौकरी मिलनी शुरू हुई तो इससे आम उपभोक्ताओं में विश्वास और उत्साह पैदा होगा। सरकार वक्त की नजाकत समझे। अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए वह दलीय भेदभाव भुलाकर सबको साथ ले और कुछ ठोस व कारगर फैसले करे। विपक्ष को भी सकारात्मक होना होगा, इस संकट के समय कोरी आलोचना से राष्ट्र अधिक संकटग्रस्त होगा।
हर नागरिक प्रतिदिन सरकार को किसी न किसी रूप में कुछ देता है और उसके दिये धन का दुरुपयोग वह सहन नहीं कर सकता। अरस्तु ने भी सावचेत किया था कि करदाता को जब यह ज्ञान होता है कि सरकार को दिये गये कर को चुनिंदे व्यक्ति और नौकरशाह अपनी समृद्धि के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं, तो करदाता इसे कत्तई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इन भ्रष्टाचार एवं बेईमानी की स्थितियों पर वर्तमान सरकार ने नकेल डाली है। उसका व्यापक असर भी देखने को मिला है।
आर्थिक सुस्ती के कारण किसी से छिपे नहीं। इन कारणों में सबसे चिंताजनक यह तथ्य सामने आना है कि उपभोक्ता खर्च कम हो रहा है। यह कमी शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में हो रही है। इसका मतलब है कि लोग भविष्य को लेकर आशंकित-भयभीत हैं और बचत करना पसंद कर रहे हैं। इससे इन्कार नहीं कि बीते दो-तीन महीनों में सरकार एक के बाद एक करीब दो दर्जन कदम उठा चुकी है और इनमें कुछ कदम ऐसे रहे जिन्हें क्रांतिकारी कहा गया, ऐसे में सरकार को कुछ ऐसे भी उपाय करने चाहिए जिससे मांग बढ़े। यह तभी होगा जब उपभोक्ता अपना खर्च बढ़ाएंगे। उचित होगा कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद व्यक्तिगत आयकर दरों में कटौती करने के साथ अन्य वे उपाय किए जाएं जिससे लोग अपनी खपत बढ़ाएं।
यह सवाल उठना भी लाजिमी है कि क्या हम मन्दी के दौर में फंस रहे हैं? विपक्षी नेता इसका कारण अभी तक नोटबन्दी व जीएसटी को बता रहे हैं। सरकार की इन आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था में एक बार ठहराव या गिरावट का आना लाजिमी था क्योंकि समूची अर्थव्यवस्था का स्वरूप आर्थिक अनुशासन के सांचे में ढाला जाना था। अब भी यदि विकास दर कम होती है तो इसका मतलब यह भी निकलता है कि काले धन की समानान्तर आर्थिक प्रणाली ध्वस्त हो रही है। नोटबन्दी का सबसे ज्यादा असर जमीन-जायदाद के क्षेत्र में पड़ा है जहां अब नकद जायदाद का खरीदना मुश्किल हो गया है और सारा काम नियमित, अनुशासित आर्थिक प्रणाली के जरिये ही हो सकता है। कम से कम बड़े-बड़े शहरों में यह परिवर्तन हुआ है परन्तु दूसरी तरफ बैंकों के कारोबार में कमी आयी है। इसका मतलब यह है कि बैंकों की ऋण देने की क्षमता में गिरावट आयी किन्तु इसे सरकार ने दुरुस्त करने की कोशिश भी की। बैंकों के पास पूंजी प्रचुरता बनाये रखने हेतु 70 हजार करोड़ रुपये की मदद दी। अतः पूंजी प्रचुरता के बावजूद बैंकों से कर्ज लेने में यदि हिचकिचाहट दर्ज हो रही है तो इसका अर्थ यह निकलता है कि ब्याज दरें ऊंची हैं, बैंकिंग प्रणाली में खामियां, भ्रष्टाचार एवं भेदभाव व्याप्त हैं, जिसकी वजह से निजी निवेशक कर्ज लेने से घबरा रहे हैं। इन प्रयत्नों के बावजूद यदि आर्थिक परिदृश्य धुंधले है तो हमें यही सोचना है कि इस वातावरण को किस तरह बदला जाये?
मोदी सरकार की उन समाजवादी योजनाओं की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा जो गरीबों के हाथ में धन की प्रचुरता को बढ़ा रही हैं और सरकारी खजाने से अधिक धन को सुलभ करा रही हैं। सरकार को जनता के जेब पर कर के रूप में हमला न करते हुए, उदार दृष्टिकोण अपनाना होगा। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस प्रकार फूल से भंवरा मधुकरी कर बिना फूल को नुकसान पहुंचाए काम चलाता है, ठीक उसी प्रकार सरकार को जनता से कर लेना चाहिए। अधिक नहीं। मनुस्मृति में कहा गया है कि सरकार को यथोचित मात्रा में ही कर लेना चाहिए अन्यथा साधारण जन तो क्या साधु-संत भी विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। हमें मितव्ययता की वृत्ति नहीं बल्कि खर्च करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना होगा, तभी हम देश की आर्थिक अस्मिता एवं अखण्डता को बचा सकते हैं। प्रेषकः