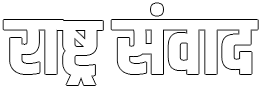राजनीति का मारक हथियार बन चुका है सोशल मीडिया
देवानंद सिंह
आज के समय में सोशल मीडिया कितना अहम हो गया है, यह सब हम और आप देख रहे हैं और महसूस भी कर रहे हैं। खबर भले ही पुष्ट ना हो लेकिन तेजी से आम लोगों तक पहुंच जा रही है। खबर रोकने की मुख्य धारा की मीडिया की परंपरा को इससे जबरदस्त झटका लगा है और यही वजह है कि सोशल मीडिया राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार बन चुका है । अन्ना आंदोलन से लेकर खाड़ी देशों के कई चर्चित आंदोलनों तक इसकी अहम भूमिका हम सबने करीब से देखी है।
अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तर राजनीतिक हथियार के तौर पर किया, यह सब हम सब ने देखा। साथ ही यह भी देखा कि किस प्रकार कुछ ही वर्षों में भारी सफलता अर्जित करने में सफलता प्राप्त की। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया और साथ ही दो राज्यों दिल्ली और पंजाब में सरकार बना ली। कई राज्यों में अपने उम्मीदवारों को संसदीय संस्थाओं में पहुंचाया।
देखा-देखी बाद में इस हथियार का इस्तेमाल सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने धड़ल्ले से करना शुरू कर दिया। कमाल तो तब हुआ जब तमाम बड़े मीडिया घराने जिनका कारोबार करोड़ों-अरबों में था, सत्ता के चारण भट्ठ बन गए और उनके करोड़ों के कारोबार करने वाले खबरिया चैनेलों को यू ट्वूब जैसे मुफ्त सेवा प्रदान करने वाले प्लेटफार्म पर कुछ हजारों की हैसियत वाले यू-ट्यूब चैनलों ने पानी पिला दिया। अपनी दर्शक संख्या उनसे भी आगे निकाल लाए। तब कार्पोरेट घरानों को सोशल मीडिया की ताकत का पता चला। कहां करोड़ों रुपयों वाले सैटेलाइट चैनल और कहां मात्र एक स्मार्ट फोन से शुरू हो सकने वाले यू-ट्यूब चैनल।
वहीं, कार्पोरेट हाउसों और व्यापारी वर्ग की बात करें तो उसे इससे रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके उत्पाद के प्रचार पर मीडिया मंच उनसे कितना भुगतान ले रहे हैं। इसपर कितना खर्च कर रहे हैं, उनका प्लेटफार्म कितना बड़ा, कितना भव्य है। उसे मतलब इस बात से रहता है कि उसके उत्पाद का प्रचार कितनी बड़ी आबादी तक पहुंच रहा है। उसका माल कितना बिक रहा है। उसके उपभोक्ताओं का दायरा किस रफ्तार से बढ़ रहा है और वह प्रचार पर जो खर्च कर रहा है उसका उसके लाभ में कितना योगदान हो रहा है। अगर हजार के निवेश वाला प्लेटफार्म अरबों के निवेश वाली सेवा कम खर्च में दे दे रहा है तो क्या जरूरत है अरबपति प्लेटफार्मों की। लिहाजा विज्ञापन का बाजार प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रोनिक मीडिया की यात्रा करता हुआ डिजिटल मीडिया तक अपनी पहुंच बना रहा है। प्रिंट और सैटेलाइट मीडिमा की हिस्सेदारी घटती जा रही है।
बता दें कि यूरोप में तो विज्ञापनों का प्रवाह पूरी तरह सोशल मीडिया की तरफ मुड़ चुका है। भारत में भी यह तेज़ी से घटित हो रहा है। ऐसे में हर बड़ा मीडिया हाउस अपने डिजिटल संस्करण को मजबूत कर रहा है। उसकी अलग टीम तैनात कर रहा है। कारण है कि आज हर दूसरे हाथ में स्मार्ट फोन है और मोबाइल कंपनियां सस्ते में भारी-भरकम डाटा की सुविधा प्रदान कर रही हैं। उंटरनेट की कोई समस्या नहीं है। उसे स्मार्ट टीवी खरीदने या सके पास बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। वह चलते फिरते कहीं भी वीडियो देख सकता है। नई-पुरानी, देशी-विदेशी फिल्में देख सकता है। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दुनिया में ताक-झांक कर सकता है। देश-दुनिया की छोटी-बड़ी सभी खबरों की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
इन सबों बातों को सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया ने यह कमाल कर दिखाया है कि महाभारत के संजय की तरह घर बैठे कोई महाभारत का युद्ध देख सकता है। उसकी बखान कर सकता है। उसके बखान को जगह देने के लिए सोशल साइटें मौजूद हैं। वह अपनी क्षमता के मुताबिक अपनी बात रख देगा जिसे देखना हो देखे, जिसे सुनना हो सुने। उसका मन तो हल्का हो ही जाता है। स्मार्ट फोन आने से पहले उसे इसके लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती थी। जो हर किसी के वश की बात नहीं थी। स्मार्ट फोन उनके रोजमर्रे के जीवन के कई कामों में मददगार साबित हो रहा है।
बहरहाल इंटरनेट और सोशल मीडिया की ताकत जिस तरह बढ़ती जा रही है हमें इस बात का बिल्कुल भ्रम नहीं रहना चाहिए कि आने वाले समय में भी सोशल मीडिया में छोटी पूंजी का अपना आकार बढ़ने का अवसर जारी रहना संभव होगा। बड़ी मछलियां जब तालाब में उतरती हैं तो छोटी मछलियों को जीने नहीं देंगी। बड़े खिलाड़ी जब सोशल मीडिया की दुनिया में उतरेंगे तो पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे। विज्ञापनों की दुनिया पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए वे कुछ भी करेंगे। भारी पूंजी झोंक कर सक्षम पत्रकारों और कुशल तकनीकिशियनों की वह फौज उतार देंगे । ऐसे में आने वाला समय साइबर जगत में भारी उथल-पुथल वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन फिलहाल इसके अंदर छोटी पूंजी का प्रवेश सुगम है। उन्हें आगे बढ़ने की पूरी आजादी है।
लेकिन किसी भी देश की सत्ता अभिव्यक्ति की इतनी ज्यादा स्वतंत्रता को बर्दाश्त नहीं करतीं। सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जहां चेक एंड बैलेंस का कोई प्रावधान नहीं है। जहां कोई भी व्यक्ति जब चाहे अपना प्रोफाइल बना सकता है। जो जी में आए लिखकर पोस्ट कर दे। पोस्ट लिखने वाला क्षेत्रीय संवाददाता से लेकर प्रधान संपादक तक की भूमिका में। कोई रोक-टोक नहीं। सोशल नेटवर्किंग साइटों का मकसद विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान का एक खुला मंच प्रदान करना था। लेकिन इतना ज्यादा खुला मंच था कि इसपर असामाजिक और शरारती तत्वों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं थी। जब इसपर सरकार की नीतियों की आलोचना होने लगी तो इनपर अंकुश लगाने के प्रयास तेज़ हुए।
भारत सरकार ने साइबर निगरानी और नियंत्रण के लिए सूचना प्राद्योगिकी अधिनियम पारित की। उसमें संशोधन किए। इसकी धारा 66-ए में प्रावधान था कि किसी आपत्तिजनक पोस्ट पर पुलिस तत्काल कार्रवाई कर सकती थी। पोस्ट डालने वाले को गिरफ्तार कर सकती थी। इस धारा का एक समय में खूब दुरुपयोग किया गया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया और स्थानीय पुलिस को इसके लिए तत्काल गिरफ्तार करने का अधिकार खत्म कर दिया। 66-ए के प्रावधानों में बदलाव करते हुए फैसला किया गया कि ऐसे मामले में गिरफ्तारी से पूर्व आईजी अथवा डीजीपी स्तर के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर सरकारी शिकंजा थोड़ा ढीला पड़ा।
इसमें कोई संदेह नहीं कि सोशल मीडिया पर एंटी सोशल तत्वों की गतिविधियां भी बेरोक-टोक चलती हैं। उनपर नियंत्रण के लिए कानून होना ही चाहिए लेकिन आम जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति और अपराधियों की साजिशों के बीच फर्क तो करना पड़ेगा। सोशल मीडिया ने आम नागरिकों को यह ताकत दी है कि यदि सरकार उनकी फरियाद को अनसुनी करती है तो अपनी बात सार्वजनिक फलक पर रख सके। उसपर रायशुमारी करा सके।
बता दें सोशल मीडिया इक्कीसवीं शताब्दी की देन है। परंतु बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में इसकी दस्तक शुरू हो गई थी। 1994 में सोशल मीडिया का पहला प्लेटफार्म जीयोसाइट आया। इसे छह शहरों में लांच किया गया। इसमें विचारों के आदान-प्रदान और संवाद की सुविधा थी। धीरे-धीरे यह दुनिया के कई देशों में फैल गया। 2002 में फ्रेंडस्टर आया। इसके बाद माई स्पेस आया। वर्ष 2004 तक दस लाख से अधिक लोग इसपर सक्रिय हो गए थे। 2008 तक एचआई-5, फ्रेंडस्टर और फेसबुक इसके प्रतिद्वंद्वी थे। इसके बाद फेसबुक, यू-ट्यूब रेडिट आदि मैदान में उतरे और अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। इन साइटों में निरंतर बदलाव होता रहता है, लेकिन स्वरूप वही रहता है। कभी फेसबुक मेटा हो जाता है तो कभी ट्यूटर एक्स बन जाता है। यह मालिकाना और प्रबंधकीय व्यवस्था में बदलाव के कारण होता है। रोज नए-नए प्लेटफार्म अवतरित और विलीन होते रहते हैं।
2016में एक नया प्लेटफार्म आया टिकटॉक। मात्र दो वर्षों के अंदर इसके 50 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हो गए। हर महीने दो करोड़ नए उपयोगकर्ता इसमें शामिल होने लगे। यह चीन का एप था। 2020 में मोदी सरकार ने इसपर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने भी इसकी नकेल कस दी। कई देशों ने इसे मैदान से बाहर कर दिया।
ऐसे कई प्रभावशाली प्लेटफॉर्म बुलबुले की तरह उठे और अचानक गायब हो गए। 2006 में माई स्पेस गूगल से भी आगे निकल गया था। लेकिन 2012 आते-आते फेसबुक से मात खा गया। एचआई-5 और फ्रेंडस्टर जैसे प्लेटफार्म भी गायब हो गए।
सोशल मीडिया के प्लेटफार्मों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ से उपयोगकर्ताओं की सुविधाओं में इजाफा होता जाता है। ट्विटर ने शुरुआत में उपयोगकर्ताओं को वीडियो या फोटे अपलोड करने की सुविधा नहीं थी। 2011 में यह सुविधा मिली। आज ट्विटर अर्थात एक्स पर अधिकांश पोस्ट के साथ फोटो और वीडियों शामिल हैं। यह राजनीति की दिशा को तय करने और बदलने की स्थिति में आ चुका है। सोशल मीडिया से हर लिंग, हर आयुवर्ग के लोग जुड़ चुके हैं। हालांकि, सामान्य तौर पर, वृद्ध लोगों की तुलना में युवा लोग अधिक जुड़े हैं।