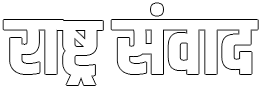भारत-पाकिस्तान तनाव और ईरान, सऊदी अरब की चिंता
देवानंद सिंह
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तीव्र तनाव पैदा कर दिया है। 26 निर्दोष नागरिकों की मौत और कई अन्य के घायल होने की इस त्रासदी के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमले के पीछे सीमापार से सक्रिय आतंकी समूहों की संलिप्तता का आरोप लगाया है।
जवाबस्वरूप भारत ने कई तीखे कदम उठाए, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, सीमा पार आवाजाही रोकना और पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द करना शामिल है। वहीं, पाकिस्तान ने इसे झूठा आरोप बताते हुए शिमला समझौते से बाहर आने की घोषणा की और भारत की किसी भी कार्रवाई को युद्ध का एलान मानने की चेतावनी दी।
यह संकट केवल भारत-पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहने वाला, इसीलिए ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों ने इस तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक मध्यस्थता की पेशकश की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची की पहल दिलचस्प है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को भाईचारे वाले पड़ोसी बताते हुए मध्यस्थता की पेशकश की और फारसी कवि सादी की कविता का हवाला देते हुए शांति की अपील की। ईरान का यह रुख केवल आदर्शवादी नहीं है, बल्कि रणनीतिक भी है।
दरअसल, ईरान-पाकिस्तान सीमा पर भी हाल के वर्षों में आतंकवादी गतिविधियानि बढ़ी हैं, जिससे तेहरान की चिंता स्वाभाविक है। वहीं, भारत के साथ उसका चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और ऊर्जा सहयोग उसे इस क्षेत्र में स्थिरता का हितधारक बनाता है। भारत अगर पाकिस्तान को बायपास कर ईरान से पश्चिम एशिया में संपर्क बनाना चाहता है, तो तेहरान के लिए नई दिल्ली से संबंध बनाए रखना आवश्यक है। ऐसे में, शांति की पहल ईरान के कूटनीतिक रुतबे को भी बढ़ाती है।
सऊदी अरब ने भी भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की है। विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने एस. जयशंकर और इसहाक़ डार दोनों से फोन पर बातचीत की। सऊदी अरब की भूमिका पिछले संकटों में भी मध्यस्थता की रही है, विशेषकर 2019 के पुलवामा हमले के बाद।
सऊदी की रणनीति भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन बनाने की रही है—एक ओर पाकिस्तान के साथ उसके धार्मिक और सैन्य संबंध हैं, वहीं भारत के साथ आर्थिक और निवेश आधारित रिश्ते। सऊदी अरब का मकसद केवल शांति स्थापित करना नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखना भी है। वह खुद को एक मूल्य आधारित मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, खासकर, ईरान के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव के मुकाबले में।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासचिव दोनों ने हमले की निंदा की और संयम बरतने की अपील की है। हालांकि, उनकी भूमिका सीमित और प्रतीकात्मक ही दिखती है। संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता इस संदर्भ में कम दिखती है, विशेषकर तब जब भारत इस संस्था के भीतर पाकिस्तान के कश्मीर पर उठाए हर मुद्दे को आंतरिक मामला कहकर खारिज करता रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर को हजारों वर्षों से लेकर लड़ते आए हैं और मुझे लगता है वे खुद हल निकाल लेंगे, इस संकट पर अमेरिका की दूरी बनाए रखने की रणनीति को दर्शाता है। हालांकि अमेरिका की राष्ट्रीय इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड ने हमले के लिए इस्लामी चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराते हुए भारत का समर्थन किया।
इस दोहरे रवैये से संकेत मिलता है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। भारत के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी और पाकिस्तान के साथ पुराने सैन्य संबंध—दोनों ही उसे एक तरफ झुकने से रोकते हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों की मध्यस्थता किसी सार्थक दिशा में जा सकती है? भू-राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर कोई ठोस कदम नहीं उठाता, भारत किसी भी मध्यस्थता को गंभीरता से नहीं लेगा।
इसके साथ ही भारत का यह भी मानना है कि द्विपक्षीय मुद्दों पर कोई तीसरी पार्टी न तो जरूरी है, न ही स्वीकार्य। शिमला समझौते और लाहौर घोषणापत्र जैसी ऐतिहासिक संधियों में यह स्पष्ट किया गया है। ऐसे में, ईरान या सऊदी की पेशकश केवल प्रतीकात्मक रह सकती है—अगर, पाकिस्तान अपनी जमीन पर सक्रिय आतंकवादी ढांचे के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता।
कुल मिलाकर, पहलगाम हमला, भारत की आक्रामक कूटनीति, पाकिस्तान की जवाबी धमकियां और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की पेशकश, सब मिलाकर दक्षिण एशिया को एक बार फिर ऐसे चौराहे पर खड़ा कर चुके हैं, जहां शांति और युद्ध दोनों की संभावनाएं समानांतर चल रही हैं। भारत की नई रणनीति पाकिस्तान को आर्थिक, कूटनीतिक और जल संसाधनों के स्तर पर घेरने की है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी अब केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों को सक्रिय करने की है। ईरान और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय ताकतों की मध्यस्थता की इच्छा उनके अपने हितों से संचालित है, न कि केवल शांति की कामना से।
ऐसे में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह संकट किसी नए संतुलन की ओर बढ़ेगा, या एक और सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट-टाइप प्रतिक्रिया में तब्दील होगा। जो तय है, वह यह कि आने वाले हफ्तों में दक्षिण एशिया की कूटनीति, सुरक्षा नीति और जल राजनीति, सभी की परीक्षा होने वाली है।