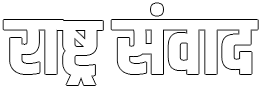संघर्षविराम पर सियासत उचित नहीं
देवानंद सिंह
भले ही, भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो गया हो, लेकिन इस पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। आरोप-प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। भारत के भीतर इसकी तुलना 1971 के भारत-पाक युद्ध और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की रणनीतिक सूझबूझ से की जाने लगी है। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस गरम है। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थकों ने इंदिरा गांधी की तस्वीरें साझा कीं, उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को दी गई कड़ी चेतावनियों का स्मरण कराया और वर्तमान सरकार की अमेरिका पर निर्भरता पर कटाक्ष किया।
यह स्वाभाविक है कि जब किसी ऐतिहासिक परिघटना की पुनरावृत्ति का आभास होता है, तो जनस्मृति उससे तुलनात्मक विश्लेषण करने लगती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 1971 की परिस्थितियों की आज से तुलना की जा सकती है? 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा जल रहा था। मानवाधिकारों का भीषण हनन, लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत की ओर पलायन कर रहे थे, और भारत पर असहनीय सामाजिक-आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। इंदिरा गांधी ने इसे केवल मानवीय संकट नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाया और सैन्य हस्तक्षेप का रास्ता अपनाया। इस युद्ध का परिणाम न केवल पाकिस्तान की सैन्य हार थी, बल्कि बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का जन्म भी हुआ। इस पूरी प्रक्रिया में सोवियत संघ भारत का मज़बूत कूटनीतिक और सामरिक साझेदार बना। वहीं, अमेरिका, विशेषकर राष्ट्रपति निक्सन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर, पाकिस्तान के जनरल याह्या खान के पक्षधर थे। अमेरिका का छुपा समर्थन पाकिस्तान के साथ था और निक्सन-इंदिरा के रिश्ते तल्ख़ थे। बावजूद इसके, इंदिरा गांधी ने अमेरिकी दबाव को दरकिनार कर निर्णायक सैन्य कार्रवाई की और न केवल भारत की गरिमा बचाई, बल्कि दक्षिण एशिया के नक्शे को बदल दिया, लेकिन, 2025 की परिस्थितियां एकदम भिन्न हैं। पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अमेरिका का प्रभाव पहले से कहीं अधिक व्यापक है, और भारत वैश्विक मंचों पर अमेरिका के साथ रणनीतिक भागीदारी को प्राथमिकता देता है। ऐसे में, किसी भी प्रकार की सैन्य कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया अधिक तीव्र होती है, और टकराव को सीमित रखना कूटनीतिक विवेक का प्रमाण माना जाता है।
ट्रंप के ट्वीट के बाद भारत सरकार द्वारा सीज़फायर की पुष्टि ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। कई लोगों ने पूछा कि क्या भारत को आज भी अमेरिका की मध्यस्थता की आवश्यकता है? क्या भारत जैसी उभरती वैश्विक शक्ति अब भी दूसरों के कहने पर रणनीतिक फैसले ले रही है? यह आलोचना तभी प्रासंगिक मानी जा सकती है, जब इसे दो कोणों से देखा जाए। पहला, क्या भारत ने यह संघर्षविराम दबाव में लिया? और दूसरा, क्या भारत ने अपनी सैन्य स्थिति को पर्याप्त मज़बूती से प्रस्तुत करने के बाद ही यह निर्णय लिया? ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत भारतीय सेना की कार्रवाई ने पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। भारतीय सेना ने खुद पुष्टि की कि छह-सात मई की रात को पाकिस्तान के कई ठिकानों पर प्रहार किए गए। इससे स्पष्ट है कि भारत ने एकतरफा दबाव में नहीं, बल्कि सामरिक बढ़त हासिल करने के बाद यह निर्णय लिया। इतना जरूर माना जा सकता है कि अमेरिका की भूमिका निर्णायक रही, लेकिन इसे ‘मध्यस्थता’ के बजाय ‘सुविधाकर्ता’ की भूमिका कहा जा सकता है।
लेकिन, कांग्रेस पार्टी ने इसे वर्तमान सरकार की कमजोरी करार देने का अवसर समझा। इंदिरा गांधी और निक्सन की पुरानी तस्वीरों से लेकर उनकी कही गई सख्त बातों को उद्धृत किया गया। एक वायरल ट्वीट में लिखा गया, वो वक़्त चला गया जब कोई देश तीन-चार हज़ार मील दूर बैठकर ये आदेश दे कि भारतीय उसकी मर्ज़ी के हिसाब से चलें। कई कांग्रेस नेताओं ने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करने की उपलब्धि को याद दिलाया और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से की, और कहा चुनाव लड़ने और युद्ध लड़ने में फर्क होता है। यूं ही कोई इंदिरा गांधी नहीं बन जाता।
इन प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति में इतिहास को वर्तमान की कसौटी पर कसने का प्रयास लगातार होता रहा है, लेकिन इसकी एक सीमा भी होनी चाहिए। इतिहास की घटनाएं संदर्भ के साथ जुड़ी होती हैं, और एक जैसे फैसलों के लिए अलग-अलग परिस्थितियों में एक जैसी प्रशंसा या आलोचना उचित नहीं। कांग्रेस के प्रहारों का जवाब बीजेपी ने भी दिया। बीजेपी ने 1971 के बाद हुए शिमला समझौते की ओर इशारा किया, जिसमें पाकिस्तान के 99,000 युद्धबंदियों को बिना किसी ठोस रणनीतिक लाभ के रिहा करने पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि, “न तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली कराने की कोई शर्त रखी गई, न ही सीमा को औपचारिक रूप से तय किया गया। न ही युद्ध या भारत पर थोपे गए शरणार्थी संकट के लिए कोई मुआवज़ा मांगा गया।
यह तर्क राजनीतिक दृष्टि से समझा जा सकता है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उस समय भारत जिस वैश्विक दबाव और सामरिक संतुलन से जूझ रहा था, उसमें निर्णय लेना आसान नहीं था। शिमला समझौता यदि एक चूक था, तो वह एक व्यापक कूटनीतिक समझौते का हिस्सा भी था। 1971 में अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी बेड़े की तैनाती एक प्रकार की धमकी थी। उस समय भारत की प्रतिक्रिया थी सोवियत नौसेना की मदद से उस चुनौती का प्रतिकार करना। आज भारत और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरह बदल चुके हैं। अब दोनों देश सामरिक साझेदार हैं, क्वाड जैसे मंचों में सहयोग कर रहे हैं, और चीन के विरुद्ध रणनीतिक रूप से एकमत हैं। ऐसे में, अमेरिका की भूमिका अब धमकी देने वाली नहीं, संतुलन बनाने वाली हो गई है। यह परिपक्वता की ओर बढ़ा एक संबंध है, न कि आत्मसमर्पण से जुड़ा कोई मामला।
कुल मिलाकर, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम स्वागतयोग्य है, बशर्ते यह स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करे। अमेरिका की भूमिका पर आलोचना हो सकती है, लेकिन वैश्विक कूटनीति में संवाद और मध्यस्थता कायरता नहीं, विवेक का प्रमाण मानी जाती है।
इंदिरा गांधी का साहस और 1971 की जीत एक स्वर्णिम अध्याय है, लेकिन वर्तमान समय की जटिलताओं को देखते हुए हमें न तो हर फैसले की तुलना उसी कसौटी पर करनी चाहिए, और न ही राजनीतिक लाभ के लिए इतिहास को हथियार बनाना चाहिए। भारतीय राजनीति को चाहिए कि वह इतिहास से प्रेरणा ले, लेकिन उसके नाम पर वर्तमान की आलोचना केवल इसलिए न करे क्योंकि वह तत्कालीन परिस्थितियों से मेल नहीं खाती। आज की भारत सरकार को चुनौतीपूर्ण वैश्विक स्थितियों में संतुलन साधते हुए आगे बढ़ना है, और वह तब तक संभव है जब राष्ट्रीय हित, गरिमा और विवेक के बीच सही तालमेल बना रहे।