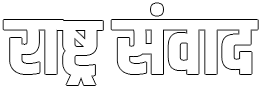देवानंद सिंह
भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे अभूतपूर्व सैन्य तनाव के बाद अचानक घोषित हुआ संघर्ष विराम भले ही दुनिया को चौंकाया हो, लेकिन यह संघर्ष विराम न सिर्फ दक्षिण एशिया की शांति के लिए राहत भरा क्षण है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि दोनों परमाणु-संपन्न देश विनाश के कगार से पीछे हटने को विवश हुए। 6 मई से 10 मई के बीच चली चार दिनों की सैन्य झड़पें, हवाई अड्डों पर हमले, मिसाइल हमले और एलओसी पर गोलाबारी एक पूर्ण युद्ध की आहट थीं। किंतु 11 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित संघर्ष विराम ने इस युद्ध की लपटों पर अस्थायी रूप से जल छिड़कने का कार्य किया। इस घटनाक्रम को केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि कूटनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी समझा जाना चाहिए।
22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया तेज़ और स्पष्ट थी। भारत ने 6-7 मई की रात पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए। इसे भारत ने केंद्रित और नपी-तुली कार्रवाई बताया, जबकि पाकिस्तान ने इसे आक्रामक माना और जवाब में बुनयान अल मरसूस नामक अभियान शुरू कर भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। दोनों देशों ने एक-दूसरे के ड्रोन व मिसाइलों को मार गिराने के दावे किए। एलओसी पर भी भीषण गोलीबारी हुई। इस स्थिति ने 1999 के करगिल युद्ध के बाद पहली बार दक्षिण एशिया को परमाणु युद्ध के करीब पहुंचा दिया।
इस तनाव के समाधान में निर्णायक भूमिका अमेरिका ने निभाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अमेरिका की मध्यस्थता से यह संघर्ष विराम संभव हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने न केवल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत की। यह मध्यस्थता केवल सामान्य कूटनीति नहीं थी, बल्कि अमेरिका के लिए एक रणनीतिक संतुलनकारी भूमिका का पुनर्प्रतिष्ठान भी था।
अमेरिका जहां भारत के साथ बढ़ते रक्षा और व्यापारिक रिश्तों से जुड़ा है, वहीं पाकिस्तान की सैन्य और आर्थिक सहायता का भी पारंपरिक स्रोत रहा है। अमेरिका की इस दोतरफा संलग्नता ने उसे एकमात्र ऐसा देश बना दिया है, जो दोनों पक्षों पर पर्याप्त प्रभाव रखता है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की ओर से दोनों देशों पर दबाव और आश्वासन का मिला-जुला संयोजन ही इस संघर्ष विराम की नींव बना, लेकिन, यह सवाल अब सबसे बड़ा है कि यह संघर्ष विराम कब तक टिकेगा ? लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि दोनों ही देशों के लिए अमेरिका महत्वपूर्ण हैं और इस तनाव को बढ़ाना उनके हित में नहीं है। वहीं रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि दोनों ही देश अपने-अपने लोगों को यह कहने की स्थिति में हैं कि उन्होंने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर हमले किए, जबकि पाकिस्तान ने जवाबी हमलों और भारतीय लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने का दावा किया। दोनों देशों को सम्मानजनक निकास की ज़रूरत थी और यह संघर्ष विराम उसी का परिणाम है।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति भारत की नीति कठोर और अविचलित है। भारत ने यह भी स्पष्ट संकेत दिए कि भविष्य में कोई भी आतंकी हमला युद्ध का कारण माना जाएगा। यह संदेश भारत के नए सैन्य सिद्धांतों की झलक देता हैं, जिसमें पारंपरिक कूटनीतिक प्रतिक्रियाओं की बजाय प्रत्यक्ष और त्वरित सैन्य उत्तर को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय सेना ने यह स्पष्ट किया कि भारत पूर्ण परिचालन सतर्कता में है, लेकिन वह तनाव नहीं बढ़ाना चाहता, बशर्ते पाकिस्तान भी इसी रास्ते पर चले। यह रुख स्पष्ट करता है कि भारत अब ‘प्रिवेंटिव डिटरेंस’ की नीति अपना चुका है, जिसमें पहले वार की नीति नहीं है, लेकिन जवाबी हमले तीव्र और निर्णायक होंगे।
उधर, पाकिस्तान के लिए यह संकट सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं था। सेना के भीतर और देश के भीतर जनभावना लगातार भारत को जवाब देने की मांग कर रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने बयान जारी कर कहा कि भारत को भरपूर जवाब दिया गया है, इससे यह प्रतीत होता है कि पाकिस्तान ने भी अपने नागरिकों को यह दिखाने का प्रयास किया कि उसने आत्मसम्मान बनाए रखा, लेकिन पाकिस्तान की असली चुनौती इसकी आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता है। आईएमएफ से ऋण, बढ़ती महंगाई, और सेना की आर्थिक निर्भरता ने उसे युद्ध की बजाय कूटनीति की ओर झुकने के लिए मजबूर किया। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सेना अब केवल सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि अपनी कूटनीतिक सूझबूझ से अपनी भूमिका को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है।
इस संघर्ष विराम ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के बीच स्थायी शांति केवल द्विपक्षीय वार्ता से संभव नहीं है। मध्यस्थता, चाहे वह अमेरिका की हो या अन्य देशों की, अब इस क्षेत्रीय संतुलन का अनिवार्य हिस्सा बन गई है। तुर्की, सऊदी अरब, ब्रिटेन जैसे देशों की भागीदारी ने यह दिखाया कि दक्षिण एशिया अब वैश्विक कूटनीतिक नेटवर्क के केंद्र में है। यह भी स्पष्ट हो रहा है कि भारत-पाक तनाव अब केवल एक द्विपक्षीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है। 12 मई यानी सोमवार को संभावित वार्ता का संकेत इस बात का संकेत है कि दोनों देश अब पीछे मुड़कर अपने विकल्पों की समीक्षा करना चाहते हैं। भारत का रुख अब भी स्पष्ट है कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान को यह निर्णय लेना होगा कि वह अपने भू-राजनीतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाता है या नहीं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संघर्ष विराम केवल एक अस्थायी राहत है। इसका स्थायित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि किन शर्तों पर सहमति बनी है। क्या पाकिस्तान ने कोई प्रतिबद्धता दी है? क्या भारत ने आगे की कार्ययोजना के संकेत दिए हैं? यह संघर्ष विराम दोनों देशों और वैश्विक समुदाय के लिए एक अवसर है। यदि, इस अवसर का उपयोग रणनीतिक धैर्य, कूटनीतिक संवाद और व्यावहारिक समझदारी के साथ किया जाए, तो यह एक नए युग की शुरुआत हो सकती है, लेकिन यदि पुरानी रंजिशें, आतंकवाद की छाया और क्षेत्रीय वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा वापस लौटती हैं, तो यह विराम एक और युद्ध का अल्पविराम बनकर रह जाएगा। भारत और पाकिस्तान को अब न सिर्फ सैन्य मोर्चों पर बल्कि वैचारिक स्तर पर भी तय करना होगा कि क्या वे 21वीं सदी में स्थायी शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं या बार-बार उसी विनाशकारी चक्र में लौटते रहेंगे।