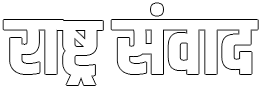नीति और प्रयोगात्मक दृष्टि से ‘क्लाउड सीडिंग’ एक साहसिक शुरुआत
देवानंद सिंह
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एक बार फिर सर्दियों के धुंधलके में डूबी है। हवा में घुलते ज़हर, घटती दृश्यता और जलती आंखों के बीच, इस बार उम्मीदें विज्ञान से थीं, आसमान से नहीं। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश यानी ‘क्लाउड सीडिंग’ का प्रयोग किया, लेकिन यह प्रयोग उम्मीदों के मुताबिक़ सफल नहीं हो सका। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह एक असफल प्रयास था, किंतु नीति और प्रयोगात्मक दृष्टि से यह एक साहसिक शुरुआत मानी जा सकती है।
मंगलवार को सेसना विमान ने पहले आईआईटी कानपुर की हवाई पट्टी और फिर मेरठ की हवाई पट्टी से उड़ान भरी। विमान ने दिल्ली के कई इलाकों खेकड़ा, बुराड़ी, उत्तरी करोल बाग़, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर के ऊपर क्लाउड सीडिंग के लिए हाइग्रोस्कोपिक नमक के फ्लेयर छोड़े, जिसका उद्देश्य था, कृत्रिम बारिश के ज़रिए वातावरण में जमे धूल और प्रदूषण के कणों को नीचे गिराना, ताकि राजधानी की हवा थोड़ी साफ़ हो सके।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस प्रयास की पुष्टि करते हुए बताया कि यह एक वैज्ञानिक प्रयोग था, जिसमें विभिन्न आर्द्रता स्तरों के अनुसार बारिश की संभावना का परीक्षण किया गया, लेकिन प्रयोग के समय वातावरण में नमी का स्तर अपेक्षाकृत बहुत कम था। यही वजह रही कि संघनन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और आसमान से पानी की बूंदें नहीं गिरीं।
आईआईटी कानपुर की टीम के नेतृत्व में हुए इस प्रयोग का वैज्ञानिक आधार सीधा है कि अगर बादलों में पर्याप्त नमी मौजूद हो और उनमें सूक्ष्म नमक या सिल्वर आयोडाइड जैसे संघनक कण छोड़े जाएं, तो वे जलवाष्प को आकर्षित कर पानी की बूंदें बना सकते हैं। जब ये बूंदें पर्याप्त भारी हो जाती हैं, तो वे बारिश के रूप में धरती पर गिरती हैं। इस प्रक्रिया को ही क्लाउड सीडिंग कहा जाता है, लेकिन विज्ञान की सफलता केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। इस परियोजना का नेतृत्व करने वाले आईआईटी कानपुर के
प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि अगर सफलता का पैमाना बारिश है, तो यह प्रयास विफल रहा। लेकिन विफलता भी प्रयोग का हिस्सा होती है। उनका कहना था कि मंगलवार को दिल्ली के आसमान में नमी की मात्रा अत्यंत कम थी। नतीजा यह हुआ कि संघनन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकी। दिल्ली में सर्दियों के मौसम में स्मॉग और प्रदूषण की परत के कारण हवा ठंडी और शुष्क हो जाती है। यह वही मौसम होता है जब हवा में नमी का स्तर गिर जाता है और ठहराव बढ़ जाता है। ऐसे में, क्लाउड सीडिंग जैसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक आर्द्रता की शर्तें पूरी नहीं हो पातीं। यानी प्रयोग का समय भले वैज्ञानिक रूप से चुना गया हो, लेकिन प्रकृति ने सहयोग नहीं दिया।
दिल्ली सरकार का दावा है कि जिन क्षेत्रों में क्लाउड सीडिंग की गई, वहां प्रदूषण के कणों, विशेष रूप से पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 और PM 10) में कुछ गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, 28 अक्तूबर के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रियल टाइम डेटा में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं दिखा। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे हवा की सफाई के स्तर पर हल्का सुधार दिखा हो, लेकिन वह मापनीय नहीं था।
यह असमानता दिखाती है कि तकनीकी प्रयोगों की सफलता केवल मशीनों से नहीं, बल्कि व्यापक पर्यावरणीय स्थितियों से भी तय होती है। दिल्ली के मामले में हवा का ठहराव, पड़ोसी राज्यों से आती पराली का धुआं और वाहन उत्सर्जन, ये सभी ऐसे तत्व हैं, जिन्हें केवल कृत्रिम बारिश से नियंत्रित नहीं किया जा सकता।दिल्ली का यह प्रयोग अपने आप में ऐतिहासिक है। यह भारत में घरेलू तकनीक से किया गया पहला क्लाउड सीडिंग प्रयास था। इससे पहले जब सूखा नियंत्रण या जल संरक्षण के लिए ऐसे प्रयास हुए थे, तब विदेशी कंपनियों और बाहरी उपकरणों का सहारा लिया गया था। इस बार प्रयोग पूरी तरह स्वदेशी तकनीक और भारतीय वैज्ञानिकों की टीम के ज़रिए किया गया। आईआईटी कानपुर में पिछले सात-आठ वर्षों से इस विषय पर शोध चल रहा है। लगभग दस वैज्ञानिकों की टीम इस तकनीक पर कार्य कर रही है। सरकार ने इसके लिए 3.21 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया। यह राशि भले ही प्रतीकात्मक लगे, लेकिन इसका संकेत स्पष्ट है, सरकार अब विज्ञान-आधारित पर्यावरण नीति की ओर बढ़ रही है।
दुनिया के कई देश पहले ही क्लाउड सीडिंग को अपने पर्यावरणीय और कृषि प्रबंधन का हिस्सा बना चुके हैं।
चीन इस तकनीक में सबसे आगे है। वहां मौसम संशोधन कार्यक्रम राज्य-स्तर पर संचालित किए जाते हैं। ड्रोन, विमान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चीन ने दसियों लाख वर्ग किलोमीटर इलाकों में कृत्रिम बारिश या बर्फबारी करवाई है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक के दौरान शहर की हवा साफ़ रखने के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। चीन का लक्ष्य था कि 2025 तक 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इस कार्यक्रम के दायरे में लाया जाए।
संयुक्त अरब अमीरात ने भी रेगिस्तानी जलवायु में बारिश बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग को नियमित नीति बना दिया है। वहां गर्मी के दिनों में दर्जनों बार विमान नमक और रसायनों का छिड़काव करते हैं, ताकि वर्षा से भूमिगत जलस्तर में सुधार हो सके। अमेरिका के पश्चिमी सूखाग्रस्त राज्यों में यह तकनीक कृषि उद्देश्यों के लिए अपनाई गई है। वहीं, सऊदी अरब ने हाल ही में इसे भूमि की उर्वरता और बंजर होते इलाकों को पुनर्जीवित करने के लिए आरंभ किया है, लेकिन इसराइल का उदाहरण यह दिखाता है कि विज्ञान की सीमाएं भी होती हैं। 1960 के दशक से इस तकनीक पर प्रयोग करने के बाद, इसराइल ने 2014 से 2021 तक बड़े पैमाने पर क्लाउड सीडिंग कार्यक्रम चलाया। सात वर्षों के अध्ययन के बाद पाया गया कि इस प्रक्रिया से वर्षा की मात्रा में कोई ठोस वृद्धि नहीं हो रही। लागत अधिक और परिणाम नगण्य थे, इसलिए इसे निलंबित कर दिया गया।
दिल्ली में हर सर्दी एक आपातकाल लेकर आती है। प्रदूषण के स्तर जब गंभीर श्रेणी में पहुंचते हैं, तब सरकारों और नागरिकों दोनों की सांसें भारी पड़ जाती हैं। ऐसे में क्लाउड सीडिंग जैसी तकनीक उम्मीद की एक किरण बनती है। पर सवाल यह है कि क्या केवल तकनीक से प्रदूषण की समस्या हल हो सकती है? उत्तर है नहीं। विज्ञान राहत दे सकता है, लेकिन समाधान नहीं। प्रदूषण का मूल स्रोत अभी भी भूमि और नीतियों में है, जैसे पराली जलाना, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण गतिविधियां और ठंड के मौसम में हवा का स्थिर हो जाना। जब तक इन पर संरचनात्मक सुधार नहीं होंगे, तब तक कृत्रिम बारिश जैसे प्रयोग अस्थायी राहत से आगे नहीं जा पाएंगे। क्लाउड सीडिंग की सबसे बड़ी चुनौती इसकी अनिश्चितता है। नमी का स्तर, बादलों की ऊंचाई, हवा की दिशा और तापमान, ये सभी कारक सफलता को प्रभावित करते हैं। दूसरे, इसकी लागत-प्रभावशीलता पर भी प्रश्न उठते हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अग्रवाल स्वयं स्वीकार करते हैं कि यह सफलता या असफलता की द्वंद्वात्मक स्थिति है। प्रयोग तब तक उपयोगी है, जब तक उससे नए निष्कर्ष निकलते रहें।
इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण के संदर्भ में यह प्रक्रिया नैतिक और पर्यावरणीय प्रश्न भी खड़ी करती है। क्या हमें वातावरण में रासायनिक पदार्थ छोड़ने से पहले उनके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन नहीं करना चाहिए? सिल्वर आयोडाइड या नमक जैसे पदार्थ वातावरण और जलस्रोतों पर क्या प्रभाव डालते हैं, यह अभी तक निर्णायक रूप से स्पष्ट नहीं है। दिल्ली सरकार का यह कदम, भले ही सीमित सफलता वाला रहा हो, लेकिन यह एक संकेत है कि सरकार अब प्रयोग करने से पीछे नहीं हट रही। आईआईटी कानपुर की टीम ने यह स्पष्ट किया है कि जैसे ही वातावरण में आर्द्रता का स्तर उपयुक्त होगा, प्रयोग दोहराया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि दिल्ली आने वाले महीनों में ऐसे और प्रयास देख सकती है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है यह समझना कि क्लाउड सीडिंग प्रदूषण नियंत्रण की प्राथमिक रणनीति नहीं, बल्कि एक पूरक उपाय होना चाहिए। वास्तविक सुधार तभी संभव होगा जब उत्सर्जन के स्रोतों पर नियंत्रण, पराली प्रबंधन में सुधार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा और उद्योगों की निगरानी जैसे ठोस कदम उठाए जाएं।
प्रदूषण नियंत्रण केवल वैज्ञानिक प्रयोगों का विषय नहीं है, यह शासन, प्रशासन और जनसहभागिता का सम्मिलित प्रयास है। विज्ञान रास्ता दिखा सकता है, परंतु निर्णय राजनीतिक इच्छाशक्ति से आते हैं। दिल्ली का उदाहरण यह बताता है कि आधुनिक तकनीकें तभी सार्थक होंगी जब वे दीर्घकालिक नीति का हिस्सा बनें। क्लाउड सीडिंग जैसी प्रक्रिया तत्कालिक राहत दे सकती है, जैसे अस्पतालों के आसपास धूल कम करना या दृश्यता सुधारना, लेकिन यह कोई स्थायी इलाज नहीं। इसे समझते हुए नीति निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी प्रयोगों के साथ-साथ पर्यावरणीय शिक्षा, सख़्त कानून और नागरिक सहयोग पर भी बराबर ज़ोर दिया जाए।
कुल मिलाकर, दिल्ली में कृत्रिम बारिश का यह पहला प्रयास असफल भले रहा, लेकिन यह असफलता निराशाजनक नहीं है। यह उस दिशा की शुरुआत है, जहां विज्ञान और शासन मिलकर पर्यावरण संकट से निपटने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। असली सफलता तब होगी जब इन प्रयोगों से मिली सीख भविष्य की नीतियों में उतरेगी। आज दिल्ली का आसमान भले ही धुएं से ढका हो, लेकिन उस धुंध में भी एक संभावनाओं की झिलमिलाहट है कि शायद एक दिन यह शहर सांस लेने लायक़ फिर से बन सके। विज्ञान की यही खूबसूरती है कि वह असफलताओं में भी आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है।