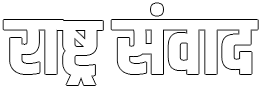नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकान्त के सामने कम नहीं चुनौतियां
देवानंद सिंह
भारत की न्यायपालिका के इतिहास में सोमवार का दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में दर्ज हुआ, जब जस्टिस सूर्यकान्त ने राष्ट्रपति भवन में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ न्यायाधीशों और उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति इस बात को रेखांकित कर रही थी कि देश की न्यायिक नेतृत्व व्यवस्था में यह बदलाव कितनी व्यापक और दूरगामी महत्ता रखता है। बीते 30 अक्तूबर को राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति की घोषणा के बाद से ही यह साफ़ था कि सूर्यकान्त का कार्यकाल सामान्य रूप से बदलने वाले तेज़-तर्रार नेतृत्व की तुलना में कहीं अधिक स्थिर और दीर्घकालिक रहने वाला है, क्योंकि वे लगभग 15 महीने तक सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व करेंगे, एक ऐसा समय, जो हाल के कई मुख्य न्यायाधीशों को उपलब्ध नहीं था। इस कारण न्यायपालिका में कई लंबित मुद्दों के समाधान की वास्तविक संभावना उनके कार्यकाल के दौरान उभर सकती है।
जस्टिस सूर्यकान्त की यात्रा एक दिलचस्प कहानी है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी, जिसने साधारण शुरुआत से उठकर देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी तक का सफर तय किया। यह यात्रा यह बताती है कि भारतीय लोकतंत्र में प्रतिभा और मेहनत कितनी निर्णायक भूमिका निभा सकती है। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में जन्मे सूर्यकान्त ने मात्र 22 वर्ष की उम्र में वकालत शुरू की। यह वह समय था जब वकालत में न तो तत्काल पहचान मिलती थी और न ही आर्थिक स्थिरता, लेकिन महज़ एक वर्ष के भीतर उन्होंने चंडीगढ़ जाकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी और आने वाले वर्षों में उन्होंने अपनी वकालत की शैली से, जिनमें प्रभावी दलीलें और तर्क-वितर्क की विशिष्ट क्षमता शामिल थी, खुद को भीड़ से अलग स्थापित कर लिया। 38 वर्ष के युवा वकील के रूप में उन्हें हरियाणा का एडवोकेट-जनरल नियुक्त किया गया, यह नियुक्ति अपने आप में एक रिकॉर्ड थी, क्योंकि इतनी कम आयु में राज्य का सर्वोच्च विधिक सलाहकार बनना उस समय लगभग अभूतपूर्व था। उनके आलोचकों ने उस समय भी उनकी योग्यता पर सवाल उठाए थे, लेकिन समय ने उनके पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि कुछ ही वर्षों बाद 2004 में वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज बनाए गए। वहां उन्होंने संवैधानिक और प्रशासनिक मामलों में अनुभव अर्जित किया और 2019 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने, जहां से उनकी सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा शुरू हुई।
हालांकि, उनकी तेजी से होती प्रगति के साथ कुछ विवाद भी जुड़े रहे, जो भारत की न्यायिक प्रणाली में पारदर्शिता के प्रश्न को लंबे समय से चुनौती देते रहे हैं। कारवां पत्रिका और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों ने उनके खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों को वर्षों पहले उजागर किया था, 2012 में एक व्यापारी द्वारा संपत्ति लेनदेन में अंडर-वैल्यूएशन के आरोप, जिसके कारण कथित तौर पर उन्होंने करोड़ों की टैक्स देनदारी से बचाव किया, और 2017 में एक कैदी द्वारा रिश्वत लेकर ज़मानत देने का आरोप। इन आरोपों की जांच और उसके परिणाम आज भी अस्पष्ट हैं, जिसके चलते न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर नए सवाल उठने अनिवार्य थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल द्वारा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र को लिखी चिट्ठी में इन मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग दर्ज की गई थी, लेकिन उस पर कभी क्या कदम उठाए गए, यह सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं। 2019 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन आरोपों को निराधार करार दिया था, परंतु पारदर्शिता की दृष्टि से यह तथ्य फिर भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी स्तर पर जांच परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए। इस पृष्ठभूमि में सूर्यकान्त की नियुक्ति न केवल न्यायालय की क्षमता और उनकी व्यक्तिगत योग्यता के सवालों के साथ आती है, बल्कि न्यायिक संस्थानों की जवाबदेही के बड़े विमर्श को भी उजागर करती है।
पिछले छह वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकान्त की भूमिका अत्यंत सक्रिय और बहुआयामी रही है। वे उन कई बड़े संवैधानिक और सार्वजनिक महत्व के मामलों की सुनवाई में शामिल रहे, जिनका प्रभाव देश की राजनीति, समाज और प्रशासनिक ढांचे पर दूरगामी पड़ा। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को चुनौती देने वाला मामला, जिसे भारत के संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मुकदमों में से एक माना जाता है, उनकी बेंच का हिस्सा था। इसी तरह राजद्रोह कानून पर पुनर्विचार, पेगासस की जासूसी से जुड़े आरोप, असम में नागरिकता पंजीकरण की प्रक्रिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी वे निर्णायक भूमिका में थे।
इन बड़े मामलों में उनकी न्यायिक शैली का एक दिलचस्प मिश्रण देखने को मिला, कभी वे राज्य की शक्ति पर प्रश्न उठाते दिखे, तो कभी न्यायिक संयम का परिचय देते हुए अत्यधिक हस्तक्षेप से बचते भी नज़र आए। उदाहरण के लिए, नूपुर शर्मा मामले में उनकी टिप्पणी अत्यंत चर्चित रही, जहां उन्होंने सभी एफआईआर को दिल्ली स्थानांतरित करके उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी, वहीं उन्होंने मौखिक टिप्पणी में यह कहा कि उनकी विवादित टिप्पणी ने देश में एक हत्या का माहौल बनाया। यह टिप्पणी राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील बन गई थी। एक ओर उनके समर्थकों ने इसे धार्मिक सौहार्द और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रश्न बताया, वहीं आलोचकों ने इसे न्यायिक मर्यादा के विरुद्ध कहा। यह विवाद भारतीय न्यायपालिका में मौखिक टिप्पणियों के प्रभाव का एक उदाहरण भी बन गया।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में सूर्यकान्त का दृष्टिकोण संतुलित प्रतीत होता है। कॉमेडियन समय रैना को कथित धार्मिक संवेदनाओं को आहत करने वाली टिप्पणियों के लिए माफी मांगने का आदेश देना उनके दृष्टिकोण में सामाजिक उत्तरदायित्व के तत्व को सामने लाता है, जबकि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली ख़ान महमूदाबाद को देशद्रोह कानून के तहत हुई गिरफ्तारी के बाद तुरंत अंतरिम जमानत देना उनके न्यायिक दृष्टिकोण के दूसरे पहलू को दिखाता है, एक ऐसा दृष्टिकोण, जो नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और राज्य की शक्ति के संतुलन में विश्वास रखता है।
उनके सबसे चर्चित निर्णयों में 2021 का वह फैसला आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि यूएपीए जैसे कठोर कानूनों के तहत एक अभियुक्त के मुकदमे की सुनवाई में अनुचित देरी हो रही हो, तो उसे जमानत दी जानी चाहिए। यह फैसला न केवल न्यायिक व्यावहारिकता को समझाता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि न्याय केवल कानून की कठोरता नहीं, बल्कि प्रक्रिया की निष्पक्षता और समयबद्धता पर भी निर्भर करता है। इस निर्णय के आधार पर कई अभियुक्तों को राहत मिली और अब भी कई मुकदमों में इसका हवाला दिया जा रहा है। यह फैसला सूर्यकान्त की न्यायिक दर्शन की बुनियादी विशेषता को सामने लाता है, ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर संतुलन साधने का प्रयास।
मुख्य न्यायाधीश के रूप में अब उनके सामने कई गंभीर और लंबित मामले हैं जो सीधे-सीधे देश के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे से जुड़े हुए हैं। नागरिकता संशोधन कानून पर दायर याचिकाएं वर्षों से कोर्ट में लंबित हैं और अब यह अपेक्षा की जा रही है कि उनके नेतृत्व में इस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। इसी प्रकार मैरिटियल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली याचिकाएं, चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा विवाद, मनी लॉन्ड्रिंग कानून की कठोरताओं पर उठे प्रश्न, रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन का मुद्दा, और बिहार में शुरू विशेष इंटेंसिव रिवीजन मॉडल को राष्ट्रव्यापी करने की मांग जैसे कई सवाल सुप्रीम कोर्ट की नज़र में हैं। इन सभी मामलों में न केवल कानूनी व्याख्याएं जटिल हैं, बल्कि इनके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम भी अत्यंत व्यापक हो सकते हैं।
इस बात को भी समझना होगा कि जस्टिस सूर्यकान्त ऐसे समय में मुख्य न्यायाधीश बने हैं जब भारत की न्यायपालिका अनेक मोर्चों पर संघर्ष कर रही है। लाखों मामलों का भारी बोझ, संवैधानिक पीठों का निष्क्रिय होना, न्यायिक नियुक्तियों को लेकर सरकार और न्यायपालिका के बीच लगातार तनाव, और सबसे बढ़कर, न्यायिक पारदर्शिता को लेकर बढ़ती सार्वजनिक चिंता। जस्टिस चंद्रचूड़ के कार्यकाल में सक्रिय रही संवैधानिक पीठों की सुनवाई बाद में धीमी हो गई थी, मगर अब सूर्यकान्त से उम्मीद है कि वे संवैधानिक महत्त्व के मामलों को प्राथमिकता देंगे और न्यायिक प्रक्रिया में गति लाएंगे।
इसके साथ ही, भारत की न्यायिक व्यवस्था में तकनीक का बढ़ता उपयोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरणों का एकीकरण भी एक उभरती आवश्यकता है। केस मैनेजमेंट सिस्टम की डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाना, मामलों की सूचीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह स्वचालित करना, और लंबित मामलों की निगरानी को अधिक वैज्ञानिक तरीके से लागू करना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूर्यकान्त का नेतृत्व वास्तविक बदलाव ला सकता है। जजों की नियुक्ति प्रक्रिया कोलेजियम प्रणाली की पारदर्शिता और जांच प्रणाली को लेकर भी समाज में बहस बढ़ रही है; सूर्यकान्त की भूमिका यहां भी महत्वपूर्ण होगी कि वे किस प्रकार इस बहस को दिशा देते हैं।
इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि सूर्यकान्त अपने कार्यकाल में न्यायपालिका की संस्थागत विश्वसनीयता को कैसे मजबूत करते हैं। जनता का विश्वास किसी भी न्यायिक ढांचे की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब न्यायपालिका राजनीति, प्रशासन और मीडिया के दबावों से ऊपर खड़ी होकर संतुलित और निर्भीक फैसले सुनाती है, तब लोकतंत्र मजबूत होता है। सूर्यकान्त के सामने इस समय वही अवसर है, वे चाहें तो आगामी वर्षों में भारतीय न्यायपालिका की दिशा तय कर सकते हैं, उसे अधिक पारदर्शी, अधिक उत्तरदायी और अधिक मानवोन्मुख बना सकते हैं।
अंततः, जस्टिस सूर्यकान्त का कार्यकाल भारतीय न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखने जा रहा है। उनकी यात्रा, उनकी क्षमताएं, उनकी आलोचनाएं और उनके निर्णय, सभी मिलकर यह तय करेंगे कि आने वाले वर्षों में भारत की न्यायपालिका किस दिशा में आगे बढ़ती है। उम्मीद यह की जा रही है कि वे न केवल लंबित मामलों के बोझ को कम करेंगे, बल्कि न्यायालय की कार्यप्रणाली में वह स्थिरता और निरंतरता भी लाएंगे, जिसकी देश को बेहद आवश्यकता है। भारत की न्यायिक संरचना इस समय संक्रमण के दौर में है, और ऐसे में सूर्यकान्त का नेतृत्व यह तय करेगा कि यह संक्रमण किस दिशा में आगे बढ़ेगा, एक अधिक विश्वसनीय, अधिक सशक्त और अधिक जनोन्मुख न्यायपालिका की ओर, या एक ऐसी प्रणाली की ओर जो स्वयं अपनी पारदर्शिता और जवाबदेही से संघर्ष कर रही हो। उनका कार्यकाल शुरू हो चुका है। चुनौतियां सामने खड़ी हैं। अब समय बताएगा कि जस्टिस सूर्यकान्त इन चुनौतियों को कैसे साधते हैं, और क्या वे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में अपनी एक अलग और यादगार पहचान स्थापित कर पाते हैं।