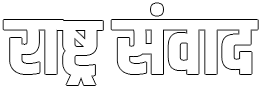विदेशी महिला खिलाड़ियों से छेड़छाड़ से देश की साख और समाज की संवेदना पर फिर उठा प्रश्नचिह
देवानंद सिंह
जून 2025 में जब अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा संबंधी सलाह जारी की और उसमें भारत को महिलाओं के लिए असुरक्षित देशों की श्रेणी में रखा, तो देशभर में तीखी प्रतिक्रिया हुई। विदेश मंत्रालय से लेकर सोशल मीडिया तक, इस एडवाइजरी को भारत की छवि पर हमला बताया गया। सरकार के समर्थक सुर में बोले कि पश्चिमी देश भारत की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच यह सिर्फ एक छवि का सवाल है, या इस एडवाइजरी के पीछे कोई सच्चाई भी है, जिसे हम स्वीकार करने से लगातार बचते आए हैं? क्योंकि, जब इंदौर और कोलकाता जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जहां एक में विदेशी महिला खिलाड़ियों के साथ सड़क पर छेड़छाड़ हुई और दूसरी में एक प्रतिष्ठित नाइट क्लब के भीतर यौन हिंसा, तो हमें यह सोचना पड़ता है कि क्या हम वास्तव में उस असुरक्षा के अंधेरे को समझना चाहते हैं, जो महिलाओं को हर रोज़ घेरता है।
इंदौर की घटना चौंकाने वाली थी, दिन के उजाले में, शहर के व्यस्त इलाके में, ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की दो खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की गई। यह कोई सुनसान सड़क नहीं थी, न ही कोई दूरस्थ कस्बा। शहर, जिसे साफ-सुथरे भारत की मिसाल बताया जाता है, वहीं ऐसी वारदात ने पूरे देश को झकझोर दिया। कुछ ही दिनों बाद, कोलकाता में एक पांच सितारा होटल के भीतर, यानी सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में, एक महिला से यौन हिंसा की घटना सामने आई। दोनों घटनाओं की समानता यही थी कि वे उस भ्रम को तोड़ देती हैं, जो हमने बड़े शहरों के बारे में पाल रखा है कि वहां महिलाएं अधिक सुरक्षित हैं। यह भ्रम उसी तरह टूटा है जैसे यह मान्यता कि शिक्षित समाज का अर्थ संवेदनशील समाज होता है। असल में, जगह कोई भी हो, मेट्रो हो या मफस्सिल, सड़क हो या स्कूल महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण लगभग एक जैसा ही रहता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.5 लाख मामले दर्ज हुए। इनमें लगभग 84 हजार मामले छेड़छाड़ के और 29 हजार से अधिक बलात्कार के थे, लेकिन आंकड़े सिर्फ गिनती नहीं बताते, वे एक मानसिकता का आईना होते हैं, ऐसी मानसिकता का, जिसमें महिला को वस्तु समझा जाता है, या उसे संस्कृति की रखवाली के नाम पर सीमित करने की कोशिश की जाती है, और यह भी याद रखना होगा कि जो मामले दर्ज होते हैं, वे पूरी तस्वीर का केवल एक हिस्सा हैं। असल संख्या कहीं अधिक भयावह है, क्योंकि समाज का एक बड़ा तबका अब भी इज़्ज़त के नाम पर चुप रहना ही बेहतर समझता है। हर बार जब कोई वीभत्स वारदात होती है, सरकारें सक्रिय दिखने लगती हैं, पुलिस जांच तेज़ करने, विशेष दल बनाने या त्वरित अदालतों के गठन की घोषणाएं होती हैं। लेकिन समानांतर रूप से, कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ऐसे बयान देते हैं, जो समस्या को और जटिल बना देते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का हालिया बयान इसका उदाहरण है, जिसमें उन्होंने पीड़िता की पोशाक और आचरण को कारण बताया। यह वही पुराना तर्क है जो अपराधियों को ढाल देता है और पीड़िताओं को दोबारा दोषी ठहराता है। सवाल यह नहीं है कि महिला क्या पहनती है या कब बाहर जाती है। सवाल यह है कि पुरुष समाज अब भी यह क्यों सोचता है कि उसे किसी महिला की आज़ादी पर टिप्पणी या नियंत्रण का अधिकार है?
राजनीति और प्रशासन का यह रवैया बताता है कि महिलाओं की सुरक्षा को अब भी विकास एजेंडा के केंद्र में नहीं रखा गया है। जब तक महिला सुरक्षा को केवल ‘लॉ एंड ऑर्डर’ का मुद्दा माना जाएगा, तब तक यह जड़ से हल नहीं हो सकता। यह सामाजिक-मानसिक बदलाव की मांग करता है, जो न शिक्षा तंत्र से जुड़ा है, न केवल पुलिस सुधार से, बल्कि हमारी परवरिश, हमारी सोच, और हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार से जुड़ा है। अक्सर, देखने में आता है कि वारदात के बाद पुलिस तंत्र सक्रिय हो जाता है। सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, दोषियों की गिरफ्तारी होती है, और फिर मीडिया का ध्यान हटते ही सब सामान्य हो जाता है, लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसे हालात बनने ही क्यों दिए जाते हैं? सुरक्षा सिर्फ किसी शहर की चौकसी या पुलिस गश्त से नहीं आती। यह उस माहौल से आती है जिसमें महिला को बराबर सम्मान मिले, चाहे वह सड़क पर चल रही हो, बस में सफर कर रही हो या खेल के मैदान में हो। भारत अब कई अंतरराष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है। जैसे—खेल, सांस्कृतिक सम्मेलन, पर्यटक उत्सव आदि, पर यदि विदेशी महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी, तो यह न केवल देश की छवि के लिए बुरा होगा बल्कि हमारे समाज की परिपक्वता पर भी प्रश्नचिह्न होगा।
अमेरिकी एडवाइजरी को हम अपमान मान सकते हैं, लेकिन वह उस वास्तविकता की ओर इशारा भी है, जिसे हम अपने भीतर जानते हैं, बस स्वीकार नहीं करना चाहते। अमेरिका ही क्यों, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की यात्रा सलाहों में भी भारत को महिलाओं के लिए हाई रिस्क डेस्टिनेशन बताया गया है। कूटनीतिक स्तर पर यह बात हमें खलती है, पर अगर, हम निष्पक्ष रूप से देखें तो यह केवल आलोचना नहीं, चेतावनी भी है कि यदि, हमने अपने समाज की सोच नहीं बदली, तो हमारी प्रगति का दावा खोखला साबित होगा। विश्वगुरु बनने की आकांक्षा तभी साकार होगी जब हमारे देश की आधी आबादी बिना डर के, सम्मान के साथ जी सके। भारतीय पुलिस व्यवस्था में महिलाओं से जुड़े अपराधों की जांच अक्सर धीमी होती है। कई राज्यों में महिला थाने तो हैं, पर उनमें पर्याप्त महिला अधिकारी नहीं। फॉरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करने की प्रक्रिया में देरी होती है, और अदालतों में मामलों के निपटारे में वर्षों लग जाते हैं।
यानी, जहां अपराधी जानता है कि सज़ा की संभावना कम है, वहीं पीड़िता को न्याय की उम्मीद लगभग नामुमकिन लगती है। यही कारण है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की पुनरावृत्ति रुक नहीं रही।
आवश्यकता है कि महिला सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के स्तर पर प्राथमिकता दी जाए, जैसे सीमाओं की सुरक्षा के लिए संसाधन जुटाए जाते हैं, वैसे ही सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा संस्कृति का निर्माण हो। यह भी मानना होगा कि महिलाओं के प्रति समाज की सोच सिर्फ परिवारों में नहीं, बल्कि मीडिया, सिनेमा और मनोरंजन उद्योग में भी आकार लेती है। फिल्मों, धारावाहिकों और गानों में जिस तरह महिलाओं को वस्तु या मनोरंजन का माध्यम दिखाया जाता है, वह दर्शकों की मानसिकता पर गहरा असर डालता है।
जब तक मनोरंजन उद्योग इस जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लेगा, तब तक संवेदनशीलता की उम्मीद अधूरी रहेगी। यह जरूरी है कि महिला किरदारों को कमज़ोरी नहीं, सशक्तता के प्रतीक के रूप में दिखाया जाए।
सरकारी नीतियां और पुलिस सुधार अपने स्थान पर जरूरी हैं, पर बदलाव की असली शुरुआत समाज से होगी। हमें यह स्वीकार करना होगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध केवल कानूनी समस्या नहीं है, यह सांस्कृतिक बीमारी है। घर में बेटे को यह सिखाना कि ना का मतलब ना होता है, स्कूलों में लैंगिक समानता की शिक्षा देना, कार्यस्थलों पर सुरक्षित माहौल बनाना, यही वह छोटे-छोटे कदम हैं, जिनसे बड़ा परिवर्तन संभव है।
हर व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, इस सामाजिक सुधार का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि महिला सुरक्षा केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं, यह पूरे समाज की आत्मा से जुड़ा प्रश्न है।
कुल मिलाकर, भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति, तीव्र आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस चमकदार उपलब्धि के पीछे जब महिलाओं की असुरक्षा की काली छाया दिखती है, तो हमारी सारी उपलब्धियां अधूरी लगती हैं। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल केवल कानून का नहीं, कर्म और चेतना का है, जब तक समाज यह नहीं समझेगा कि महिला की स्वतंत्रता पर नियंत्रण नहीं, सम्मान होना चाहिए, तब तक कोई एडवाइजरी, कोई कड़ा कानून या कोई अंतरराष्ट्रीय आयोजन हमें सुरक्षित देश नहीं बना पाएगा। भारत की असली प्रगति तब होगी जब एक लड़की रात में भी उसी आत्मविश्वास के साथ घर लौट सके, जिस आत्मविश्वास के साथ दिन में जाती है।
इंदौर और कोलकाता की घटनाएं सिर्फ दो शहरों की कहानी नहीं, वे पूरे भारत की चेतावनी हैं कि यदि, हमने अब भी नहीं सीखा, तो हर नया हादसा हमें बार-बार शर्मसार करता रहेगा।