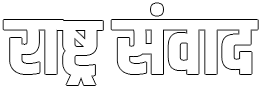*एक देश, एक चुनाव को सफल बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता*
देवानंद सिंह
भारत में ‘एक देश, एक चुनाव’ की अवधारणा फिर से चर्चा का विषय बन गई है। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी ने इस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे अब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि कोविंद समिति ने साल की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को सौंपी थी। 191 दिनों में तैयार 18,626 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2029 से देश में पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसके बाद 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के चुनाव कराए जा सकते हैं। कोविंद समिति ने यह भी कहा कि 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए हैं। अब जब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है तो ऐसी उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को आगामी शीतकालीन सत्र में संसद में पेश कर दिया जाएगा। जब इस मामले में सरकार के कदम आगे बढ़ ही रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में यह विषय न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि इसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी व्यापक हो सकते हैं।
दरअसल, ‘एक देश, एक चुनाव’ का अर्थ है कि केंद्र और राज्यों की सभी चुनावी प्रक्रिया एक ही समय पर आयोजित की जाए। वर्तमान में, भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में चुनाव समय-समय पर होते रहते हैं, जिससे चुनावी गतिविधियां देश में लगातार चलती रहती हैं। इस प्रक्रिया में कई खर्चे, संसाधनों का अपव्यय और प्रशासनिक चुनौती बढ़ जाती है। यदि, चुनाव एक साथ होंगे, तो इससे चुनावी खर्च में कमी आ सकती है, प्रशासनिक कार्यभार कम होगा और मतदाता की रुचि भी बनी रहेगी।
दूसरा, एक साथ चुनाव कराने से केंद्र और राज्य सरकारों पर भी चुनावी खर्चों का लोड कम होगा। यह सच है कि चुनावी प्रक्रिया में लगने वाले समय और संसाधनों को समेकित करने से सरकारी तंत्र पर दबाव कम होगा। इसके अलावा, विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि चुनावी समय में राजनीतिक दलों का ध्यान अपने प्रचार पर केंद्रित रहता है, इससे दीर्घकालिक विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, एक साथ चुनाव होने से राजनीतिक स्थिरता भी आएगी। अगर, केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ होते हैं, तो यह संभावित रूप से चुनावी परिणामों को स्थिरता प्रदान कर सकता है। यह सरकारों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए अधिक अधिकार और समर्थन दे सकता है, जिससे वे अपने विकास कार्यों को बेहतर तरीके से लागू कर सकें, हालांकि, ‘एक देश, एक चुनाव’ की इस अवधारणा के साथ कई चुनौतियां भी हैं।
सबसे पहले, भारत की विविधता और विभिन्न राजनीतिक दलों की अलग-अलग प्राथमिकताएं इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। विभिन्न राज्यों में स्थानीय मुद्दों और राजनीति का महत्व होता है, जिसे एक ही चुनाव में समाहित करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा, यह भी आवश्यक है कि चुनाव आयोग के पास इतनी क्षमता हो कि वह एक साथ चुनाव कराने की सभी व्यवस्थाएं कर सके। यह सुनिश्चित करना कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हों, इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।संविधान के तहत, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनावों का अलग-अलग प्रावधान है, इसलिए इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। यह प्रक्रिया जटिल और समय-कंज्यूमिंग हो सकती है और इसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
आजादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए। तब लोकसभा के साथ ही सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी संपन्न हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए गए। 1968-69 के बाद यह सिलसिला टूट गया, क्योंकि कुछ विधानसभाएं विभिन्न कारणों से भंग कर दी गई थीं।
जब साथ चुनाव कराने के लिए भंग की गई विधानसभा
कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में मद्रास के क्षेत्रों को काटकर किया गया था। उस वक्त इसमें 190 सीटों की विधानसभा थी। आंध्र प्रदेश में पहले राज्य विधान सभा चुनाव फरवरी 1955 में हुए। दूसरे आम निर्वाचन 1957 में हुए। 1957 में, सात राज्य विधान सभाओं (बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल) का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त नहीं हुआ। सभी राज्य विधान सभाओं को भंग कर दिया गया ताकि साथ-साथ चुनाव हो सके।’ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 को 1956 में पारित किया गया था। एक साल पश्चात् दूसरा आम निर्वाचन 1957 में हुआ, इसलिए आगे भी एक साथ चुनाव कराए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
कुल मिलाकर वर्तमान परिदृश्य को देखकर यही कहा जा सकता है कि, ‘एक देश, एक चुनाव’ की अवधारणा में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके लिए न केवल राजनीतिक सहमति की आवश्यकता है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया की सभी जटिलताओं को समझने और उन्हें सुलझाने की भी जरूरत है। आखिरकार, यदि यह प्रक्रिया सही ढंग से लागू होती है, तो यह न केवल चुनावी खर्चों को कम कर सकती है, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को भी मजबूत कर सकती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि सभी हितधारकों के बीच संवाद और सहमति बनी रहे, ताकि यह प्रक्रिया सभी के लिए लाभदायक हो सके।